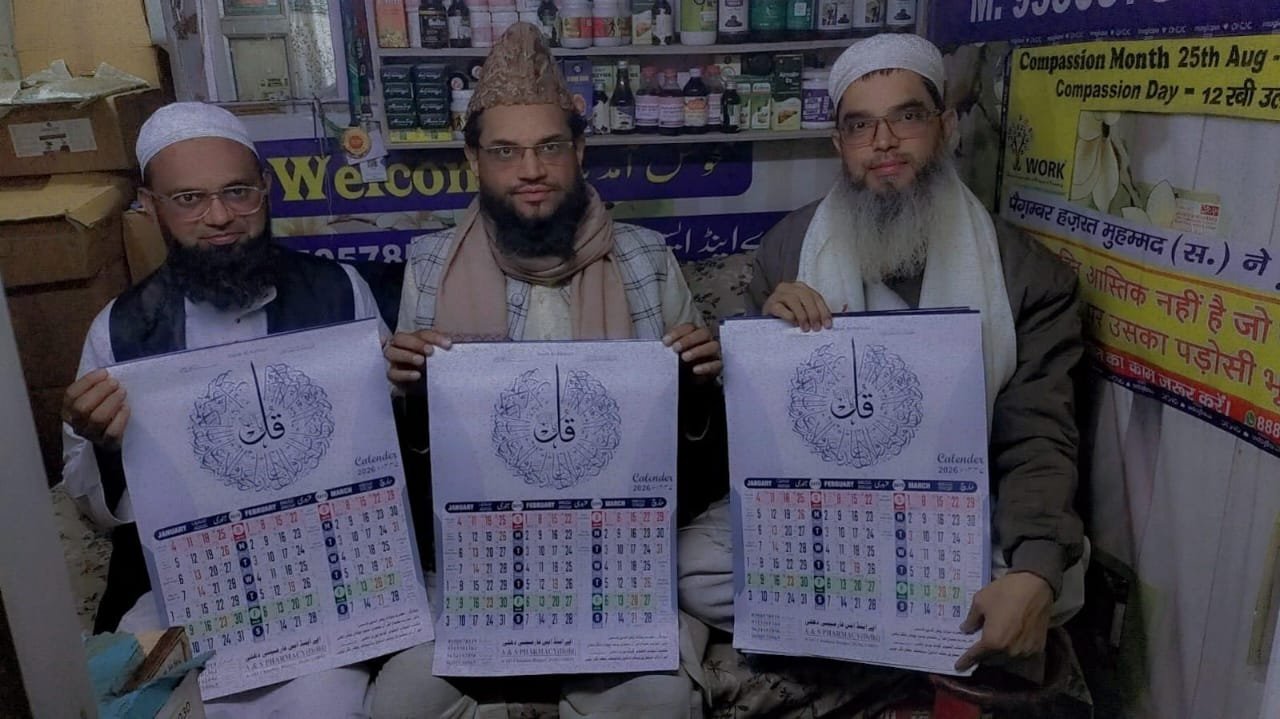डॉ. नाज़ परवीन
विश्व स्वास्थ्य संगठन के पहले महानिदेशक ब्रॉक चिशोम, (जो एक मनोरोग चिकित्सक भी थे) का कहना था कि ‘बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता’। कोविड-19 महामारी ने लगभग दो वर्षों से तबाही का जो मंजर खड़ा किया है उससे उबरने और संभलने में बेशक हमें दो- चार साल लगें, लेकिन इस महामारी ने जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर छोड़ा है, वह शायद ही कोई अपने जीवन में भूल पायेगा। निश्चित तौर पर हमारे सामने महामारी का ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। हाँ, इतिहास जरूर गवाही देता है की ऐसे संकट पहले भी आये हैं लेकिन हमारी सदी के लोगों के लिए यह खौफनाक अनुभव बिल्कुल नया ही है। जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर ना मिट पाने वाला प्रभाव डाल रहा है।
आम तौर पर छोटी-मोटी बीमारी भी चिंता बढ़ाने वाली होती है, पर जब कोई बीमारी महामारी बन कर वैश्विक आपदा के रूप में कहर बरपाए तो पूरी दुनिया को चिंता होना वाजिब है। कोरोना महामारी ने विश्व समुदाय के माथे पर ना सिर्फ चिंता की लकीरें खींची हैं अपितु एक दूसरे का मुंह तकने पर मजबूर भी कर दिया है। दुनिया की महाशक्तियाँ इस समस्या से बचने या निकलने की जद्दोजहद में दिन रात लगी हुई हैं।
महामारी का संकट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता का बड़ा कारण है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी चिंता जाहिर कर कहा था कि ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की दशकों से उपेक्षा और कमजोरी के बाद, कोविड -19 महामारी अब परिवारों और समुदायों में अतिरिक्त मानसिक तनाव पैदा करके उनको खतरे में डाल रही है।’ उनका मानना है कि महामारी नियंत्रण में आने के बाद भी दुःख, चिंता और अवसाद लोगों को प्रभावित करेंगे।
कोरोना काल की अनेक घटनाएं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति सचेत कर रही हैं। बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्या का अहम् कारण बन रहा है। कोरोना संकट के दौरान आत्महत्या के मामलों में तेजी से उछाल आया है। कुछ आर्थिक तंगी और भविष्य के संकट को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं तो कुछ महामारी के भय से मृत्यु को गले लगा रहे हैं। विशेषज्ञों की मानें तो 93 प्रतिशत आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने से ही होती हैं। सामाजिक ताने-बाने में हम उसे कोई भी नाम क्यों न दे दें, समस्या का मूल कारण मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना ही होता है।
इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अध्ययन के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण देश में शुरुआती कुछ हफ्तों में ही मानसिक रोगों के मरीजों की संख्या में 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा देखने को मिला था। महामारी ने समाज में कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। सामाजिक संबधों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। लोग अपने असुरक्षित भविष्य को लेकर चिंता में हैं। ऐसे में कोरोना ने सभी की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ा दी हैं। बच्चें, बूढ़े, नौजवान अपने भविष्य को लेकर दहशत में हैं। ऐसे में पहले से बीमार लोगों की समस्या तो और बढ़ गई है।
किसी भी वैश्विक महामारी का इतिहास इस बात की तसदीक करता है कि महामारी केवल मानव के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करती अपितु उसका खामियाजा सामाजिक ताने-बाने को भी भुगतना पड़ता है। यदि समाजार्थिक बदलाव होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोविड-19 के दौरान भी दुनिया भर में ऐसे संकेत देखे जा सकते हैं। लोगों में इस सवाल को ले कर दहशत है कि आखिर इस महामारी से दुनिया कब निज़ात पाएगी? आने वाला भविष्य कैसा होगा? महामारी से जुड़े ऐसे तमाम सवाल मानसिक दबाव पैदा कर रहे हैं।
निःसंदेह कोरोना महामारी 21वीं सदी में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन वैश्विक इतिहास में ऐसी कई महामारियां दर्ज हैं जिन्होंने मानव जाति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बड़े संकट पैदा किए हैं। हैजा, प्लेग, चिकनपॉक्स, स्पेनिश इनफ्लुएंजा आदि इतिहास की ऐसी महामारियां हैं जिनका असर अब तक देखा जा सकता है। सन 541 में फैले जस्टीनियन प्लेग को इतिहास की सबसे भयावह महामारी के रूप में याद किया जाता है। मिस्र में जन्मी इस महामारी ने देखते-देखते भूमध्य सागर से लेकर यूनानी साम्राज्य तक अपना कहर बरपाया था। इससे लगभग पांच करोड़ लोगों ने अपनी जान गँवाई थी। कहा जाता है कि आगामी दो सदियां इस बीमारी के आते-जाते प्रभाव की गवाह बनीं और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा।
14वीं सदी की महामारी ‘द ब्लैक डेथ’ ने अकेले यूरोप में लगभग दो करोड़ लोगों की जान ले ली थी। सन् 1855 में प्लेग की शुरूआत चीन से हुई और भारत में इसका रौद्र रूप देखने को मिला। इसके कारण तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के हाथ-पैर फूल गए थे। 20वीं सदी का स्पेनिश फ्लू प्रथम विश्व युद्ध में कुछ सैनिकों के संक्रमित होने से फैला था। 1918 में जन्मी इस महामारी ने लगभग 50 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था जो उस दौर में दुनिया की आबादी का एक चैथाई हिस्सा था। इसमें मरने वालों का आंकड़ा पांच करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। एक अनुमान के अनुसार, भारत में ही लगभग एक करोड़ बीस लाख लोगों ने अपनी जान गँवाई थी। त्रासदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के इतिहास में 1911 और 1921 के बीच का दशक एकमात्र ऐसा जनगणना काल रहा जिसमें भारत की आबादी का ग्राफ नीचे आ गया था। इन महामारियों ने अपने-अपने समय में मानसिक स्वास्थ्य को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। स्पेनिश फ्लू के प्रभाव से तो बाहर आने में लोगों को दशक लग गए थे।
2003 में सार्स के प्रकोप का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने बीमारी के कारण आने वाली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को रेखांकित किया जिसमें तनाव, अवसाद, मनोविकृति, पैनिक अटैक आदि को बढ़ते हुए देखा गया था। दुनिया भर में कोरोना महामारी के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों पर लगातार शोध हो रहे हैं।
एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता न होने के कारण अधिकांश लोग अपना इलाज ही नहीं करा पाते। भारतीय समाज में मानसिक रोगों के प्रति लापरवाही इस कारण भी ज्यादा है कि समाज ज्यादातर मानसिक रोगियों को पागल ही समझता है। इसका सीधा परिणाम रोगी को भुगतना पड़ता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। कई मामलों में ठीक होने पर भी ऐसे व्यक्तियों का आत्मविश्वास पूर्व की भांति नहीं लौटता। बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक अवहेलना अहम् रोल निभाती है।
डब्ल्यूएचओ की मानें तो विश्व में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी भारत में पहले से ही हैं। ऐसे में महामारी से उपजे संकट का अनुमान लगाना मुश्किल है। मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण ही भारत को ‘वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री’ की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरी ओर, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जितने मनोचिकित्सक होने चाहिए, उतने नहीं हैं। आंकड़ों की मानें तो प्रति लाख जनसंख्या पर देश में मात्र एक मनोचिकित्सक मौजूद है जबकि डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के अनुसार, प्रति लाख लोगों पर कम से कम तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए।
ऐसे में महामारी के इस संकट भरे दौर में हमें और भी सचेत रहने की आवश्यकता है। महामारी में अंगिनत लोगों ने अपने अपनों को दम तोड़ते देखा है, बहुत से लोगों की दुनिया तबाह हो गयी है। संकट की इस घड़ी में समाज और सरकार को मिलकर लोगों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस महामारी पर विजय प्राप्त की जा सके।

डॉ. नाज़ परवीन